"ऐ मुसाफिर, कहां जा रहे हैं? थक गए होंगे, दस मिनट आराम कर लीजिए। चाय-पानी पीते जाइए।"
रात के करीब दो-ढाई बज रहे हैं और बाबू जी अपने तफरीह के पलों के लिए दोस्त जुगाड़ रहे हैं। अधिकतर तो चाय-पानी के प्रलोभन में ही ठहर जाते हैं, पर कुछ ढीठ टाइप के मुसाफिरों को अलग तरीके से घेरना पड़ता है।
"लंच का टाइम हो गया है, सब अपना-अपना कलेवा खोलकर साथ में खा लीजिए।" - फिर संस्कृत का एक श्लोक, जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि साथ-साथ खाने मैं ही जीवन की सार्थकता है और सनातन धर्म का मूल भी इसी में टिका है!
ब्लोअर को बिल्कुल बेड के पास खिसकाते हुए सर्दी की रातों का अमोघ अस्त्र भी चला देते हैं - " बिल्कुल कंपकपाती ठंढ है। यहां तो अलाव भी जल रहा है। तनिक बैठ तो जाइए, देह गरम हो जाएगा।"
लगता है, कुनबे में पांच-सात जने जुड़ गए हैं, क्योंकि हुलसते स्वर में दरवाजे की तरफ मुंह कर ऊंची आवाज में सात-आठ चाय लाने का फरमान भेज दिया। फिर दुनिया-जहान की बातें शुरू होती है। कभी गाँव के बचपन के किस्से, तो कभी कितनी तकलीफों से अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी की, उसके किस्से। बकौल बाबूजी उनके जीवन की दो ही उपलब्धियाँ रही हैं - उनकी पढ़ाई और उनके बच्चे।
उनके पिताजी (मेरे दादाजी) खुद तो शिक्षक थे, शिक्षा का मोल भी समझते थे। पर बड़े परिवार को चलाने के खर्चे और ब्रिटिश इंडिया में मिल रहे मासिक तनख्वाह की रकम ने इन मूल्यों को थोड़ा व्यवहारिक बना दिया था। सो आठवीं क्लास के बाद उन्होंने अपने हाथ खींच लिए थे और स्वतंत्र कर दिया था कि आगे पढ़ाई करना है तो खुद व्यवस्था कर लो। और मजे की बात तो सुनो- जिम्मेदारी का बोझ महसूस करवाने के लिए आठवीं क्लास में शादी भी करवा दी थी!
बाबा (दादाजी) की अपनी रणनीति थी। इंडस्ट्रियल एरिया में बसे मेरे गाँव के लड़कों को उस समय नौकरी पाने में कोई विशेष तकलीफ नहीं थी। जिनकी भी जमीन का अधिग्रहण होता था, उस घर के सभी लड़कों को "नौकरी" मिल जाती थी। सो पिता जहाँ चतुर्थ वर्ग के एक नौकरी का जुगाड़ कर रहा था, बेटे के मन में आगे पढ़ने की धुन सवार थी। पिता-पुत्र के वैचारिक द्वन्द की एक ही परिणति होनी थी - बेटा घर छोड़कर बेगूसराय भाग गया!

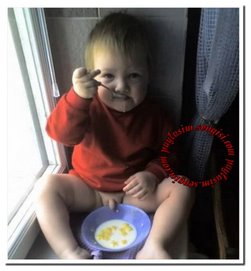
No comments:
Post a Comment