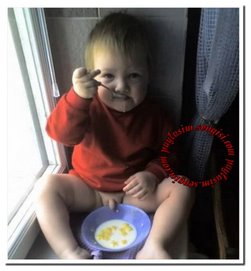(१)
मैं एक ठेलेवाला,
जन्म लेते ही पता चला/कि
ठेला खींचना ही है/
मेरी नियति -
सो घर से निकाला ठेला/
सवारी नही थी कोई ;
खाली ठेला दौड़ाता जा रहा था ।
कुछ पल बाद आभास हुआ/
संग मेरे कोई / दौड़ते चल रहा है;
मैने हवा मे सवाल दागा,
जबाब आया-
मै हूँ तुम्हारी जिन्दगी...।
(२)
मै एक ठेलेवाला,
ठेला खींचना मेरा काम;
पर यूँ ही / कब तक /
खाली ठेला लेकर दौड़ता रहता ?
एक जगह रूका,
सवारी की तलाश मे/ नजरें दौड़ाई-
पर दूर तक कोई /
ठेले के इन्तजार मे/
कोई नही था !
लगा -
इस बस्ती मे /शायद / सबके पास /
अपने-अपने ठेले हैं ।
पर /
मेरा आत्म-दंभ !
एक मिथ्या अहं !
बाध्य कर रहा था / मुझे /
कोई बोझ लेने को,
खुद को साबित करने को -
सो/
खुद को बैठा /ठेले पर /
खींचना शुरू किया ।
कि/
जिन्दगी ने अपना पाला बदला,
मूक दर्शक अब मुखर हो गया
और मजबूर करने लगा/ मुझे
संग अपने दौड़ने को ।
मैने इन्कार किया,
अपनी ही चाल चलना चाहा,
कि-
अचानक बदन पे एक कोड़ा आ पड़ा,
दर्द की तड़प मे / मैने देखा -
जिन्दगी का हाथ /
हवा मे लहराकर /
वापस आ रहा था ।
(३)
मै एक ठेलेवाला,
खींचे जा रहा हूँ ठेला/
खुद को उसपे बिठाकर ।
कोशिश कर रहा हूँ/
साथ चलने की -
जिन्दगी के साथ /
जो बाजू मे दौड़ती जा रही है,
और रह-रह कर /
मेरी सुस्त चाल देख /
कोड़े बरसाती जा रही है ।
काश!
वो समझ पाती /
कि-
ये सुस्ती नही ,अशक्तता है ,
नाटक नही , विवशता है......।
काश!
मै भी ये समझ पाता
कि/वो
ये नही समझ सकती ........।
(४)
मै एक ठेलेवाला,
खींचे जा रहा था ठेला /
खुद को उसपे बिठाकर ।
पुरानी नीली धारियों पे/ स्याह-सुर्ख
लाल रंग आते जा रहे थे ,
मेरे तन पे/
कोड़ो के /नए-नए
निशान पड़ते जा रहे थे ।
बेचारगी थी ! मजबूरी थी !
सो/
जिन्दगी का साथ /
छोड़ नही सकता था,
पर यूँ जिन्दगी भर /
कोड़े भी तो /
खा नही सकता था ।
एक पल रूका....
जिन्दगी का कोड़े वाला हाथ/
जब तक /
हवा मे लहराता/
तब तक/
मै चढ ठेले पे,
एक ही लात मे/
गिरा दिया खुद को/
अपने ठेले से ।
फिर जिन्दगी मुस्करा दी....
ठेला दौड़ पड़ा.........।
उपसंहार
सोच रहा था -
गर मै ना होंऊँ ,
ये जिन्दगी भी ना हो,
और
हम दोनो को जोड़ती/ साँसो की
डोर भी गायब हो जाए -
तो/ इस
ठेले का क्या होगा ?
पर पुरखे कहा करते हैं -
ठेला तो यूँ ही रहेगा,
दौड़ता हुआ ........
अजल के पहले भी
अबद के बाद भी
Thursday, June 21, 2007
चार सोपान : जीवन के
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
Wednesday, June 13, 2007
बचपन
बचपन में /याद है/ यूँ ही/
सादे कागज पे,
कुछ चेहरे बनाता था मै.....।
वो चेहरे -
कुछ लगते थे मुस्कराते/
कुछ गम के गीत गाते..।
ओठ उपर को खींच देता/
जब लगने होते थे हँसते ,
उलट नीचे को खींच लेता/
जब चेहरे थे रोते होते ।
थी इक बात /
पर उनमें ,
या तो वो खुश रहते /
या होते थे गम मे रोते ..।
आज याद आया /फिर से /
बचपन का वो शगल ,
कागज लिया /कलम उठाई /
मेरा मन उठा मचल ,
बनाने बैठ गया मैं चेहरे -
गोला इक खींचा/आँखे जड़ दी /
नथुनों के फैलाव बनाए।
जब ओठो की बारी आई,
बस/
सीधी रेखा सी खींच आई।
सीधी स्मित रेखा -
जो ना जा उपर /
मुस्कराहट का गुमान देती ,
ना नीचे मुड़ /
बेइंतहा गम का पैगाम देती।
कैसे बनाऊँ अब चेहरे/जो
बयाँ कर ना पाते हों /
खुद को ,
कोई अक्स बनने ना पाता है/
सामने आइने के करो गर/
उनको।
गलती नहीं है उनकी यारों /
चित्रकार ही ठहर गया है ,
दर्पण मे मैं नही दिखता /
वो बच्चा शायद मर गया है ।
सादे कागज पे,
कुछ चेहरे बनाता था मै.....।
वो चेहरे -
कुछ लगते थे मुस्कराते/
कुछ गम के गीत गाते..।
ओठ उपर को खींच देता/
जब लगने होते थे हँसते ,
उलट नीचे को खींच लेता/
जब चेहरे थे रोते होते ।
थी इक बात /
पर उनमें ,
या तो वो खुश रहते /
या होते थे गम मे रोते ..।
आज याद आया /फिर से /
बचपन का वो शगल ,
कागज लिया /कलम उठाई /
मेरा मन उठा मचल ,
बनाने बैठ गया मैं चेहरे -
गोला इक खींचा/आँखे जड़ दी /
नथुनों के फैलाव बनाए।
जब ओठो की बारी आई,
बस/
सीधी रेखा सी खींच आई।
सीधी स्मित रेखा -
जो ना जा उपर /
मुस्कराहट का गुमान देती ,
ना नीचे मुड़ /
बेइंतहा गम का पैगाम देती।
कैसे बनाऊँ अब चेहरे/जो
बयाँ कर ना पाते हों /
खुद को ,
कोई अक्स बनने ना पाता है/
सामने आइने के करो गर/
उनको।
गलती नहीं है उनकी यारों /
चित्रकार ही ठहर गया है ,
दर्पण मे मैं नही दिखता /
वो बच्चा शायद मर गया है ।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
आँगन
अपने आँगन में बैठा/
अमरूद की छाह तले /
सूरज की किरणो से/ आँखमिचौली
खेलता था मै,
चटाइ के गलीचे पे लेटा/
चाँदनी की बारिश मे / भींगता -भींगता
नहाता था मै ।
पता नही कब/
वक्त की कारीगरी ने/
डाल दिया एक छत
मेरे आँगन के उपर/
और
मुझसे मेरा आँगन छिन लिया....।
काश वो जान पाता / कि
छत आसमान नही होता है,
उसमे चँदा और सूरज नही उगते हैं...।
अब / आसमान को देखने के लिए /
धूप और चाँदनी से मिलने के लिए/
मुझे घर के बाहर
आना पड़ता है-
असुरक्षा का लबादा पहने/
जमाने से नजरें चुराए।
कल लेटा-लेटा /
छत के पार के आसमान को /
देखने की कोशिश कर रहा था ,
कि
एक पंछी आया/
कानो मे बोल गया -
मेरा खुला आस्मां लौटा दो....,
कि
एक बच्चे ने मुझे
झकझोड़ कर जगाया -
मेरा वाला आँगन लौटा दो....।
तभी /घरवाले बोल उठे -
"ये क्या आँगन मे पड़े रहते हो/
कोइ पंछी हो या बच्चे हो "
एक आवाज मेरे अंदर गूँजी-
"नहीं !
मैं छत वाले आँगन
का बाशिंदा हूँ/ और हाल ही में/
एक पंछी और एक बच्चा /
कहीं दूर दफना आया हूँ ।"
अमरूद की छाह तले /
सूरज की किरणो से/ आँखमिचौली
खेलता था मै,
चटाइ के गलीचे पे लेटा/
चाँदनी की बारिश मे / भींगता -भींगता
नहाता था मै ।
पता नही कब/
वक्त की कारीगरी ने/
डाल दिया एक छत
मेरे आँगन के उपर/
और
मुझसे मेरा आँगन छिन लिया....।
काश वो जान पाता / कि
छत आसमान नही होता है,
उसमे चँदा और सूरज नही उगते हैं...।
अब / आसमान को देखने के लिए /
धूप और चाँदनी से मिलने के लिए/
मुझे घर के बाहर
आना पड़ता है-
असुरक्षा का लबादा पहने/
जमाने से नजरें चुराए।
कल लेटा-लेटा /
छत के पार के आसमान को /
देखने की कोशिश कर रहा था ,
कि
एक पंछी आया/
कानो मे बोल गया -
मेरा खुला आस्मां लौटा दो....,
कि
एक बच्चे ने मुझे
झकझोड़ कर जगाया -
मेरा वाला आँगन लौटा दो....।
तभी /घरवाले बोल उठे -
"ये क्या आँगन मे पड़े रहते हो/
कोइ पंछी हो या बच्चे हो "
एक आवाज मेरे अंदर गूँजी-
"नहीं !
मैं छत वाले आँगन
का बाशिंदा हूँ/ और हाल ही में/
एक पंछी और एक बच्चा /
कहीं दूर दफना आया हूँ ।"
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
Monday, June 11, 2007
शहर और आदमी
एक मुर्दा शहर में/
साँस लेती हुई
लाशें रहा करती थीं ।
एक रोज /
मौत भरी फिजां से तंग आकर
सोचा सबने -
ये मरा हुआ शहर छोड़ दें
कहीं और जा /कोई जिन्दा शहर बसाएँ ।
एक जगह दिखी / निर्जन, वीरान फिजां मे
जिन्दगी मुस्करा रही थी......
सब आ वहीं बस गये ।
सुना /
फिर
वो शहर भी मर गया था।
साँस लेती हुई
लाशें रहा करती थीं ।
एक रोज /
मौत भरी फिजां से तंग आकर
सोचा सबने -
ये मरा हुआ शहर छोड़ दें
कहीं और जा /कोई जिन्दा शहर बसाएँ ।
एक जगह दिखी / निर्जन, वीरान फिजां मे
जिन्दगी मुस्करा रही थी......
सब आ वहीं बस गये ।
सुना /
फिर
वो शहर भी मर गया था।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
मेरा मस्तिष्क : मेरे विचार
हर सुबह और शाम
शुरू होती है प्रक्रिया -
अंगीठी जलाने की ।
सुलगा उसे/
अपने घर के
बाहर निकाल रख देता हूँ,
फिर धुँआ
पड़ोसी की खिड़की पार कर
उसकी सुबह कुछ साँवला बना देता है,
शाम का थोड़ा अंधेरा बढा देता है...।
पर भले हैं वो,
कुछ नही कहते,
शायद /
आदत पड़ गई है उन्हे-
इसी तरह जीने की,
उस धुँए को साँस लेने की.....।
कुछ ज्यादा दग्ध हो जाता हूँ /
जबअंगीठी तपने लगती है पूरी -
फिर जलते कोयले निकाल /
कागज मे रखता हूँ,
औरबाहर फेंक देता हूँ ...।
यकीन मानों !
वो कागज खुद नही जलते,
जलते कोयले / अपने तन पे संजोए/
सबको जलाते रहते हैं ।
बाहर दुनियाँ तपती जाती है,
अन्दर अंगीठी ठंढाती जाती है...।
शुरू होती है प्रक्रिया -
अंगीठी जलाने की ।
सुलगा उसे/
अपने घर के
बाहर निकाल रख देता हूँ,
फिर धुँआ
पड़ोसी की खिड़की पार कर
उसकी सुबह कुछ साँवला बना देता है,
शाम का थोड़ा अंधेरा बढा देता है...।
पर भले हैं वो,
कुछ नही कहते,
शायद /
आदत पड़ गई है उन्हे-
इसी तरह जीने की,
उस धुँए को साँस लेने की.....।
कुछ ज्यादा दग्ध हो जाता हूँ /
जबअंगीठी तपने लगती है पूरी -
फिर जलते कोयले निकाल /
कागज मे रखता हूँ,
औरबाहर फेंक देता हूँ ...।
यकीन मानों !
वो कागज खुद नही जलते,
जलते कोयले / अपने तन पे संजोए/
सबको जलाते रहते हैं ।
बाहर दुनियाँ तपती जाती है,
अन्दर अंगीठी ठंढाती जाती है...।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
मुर्दों की ख्वाहिश
मैं अपनी मुर्दा नज्मों को
जलाता नही/
जमीन मे गाड़ता नही/
ताबूतों मे भी कैद नही करता ;
छोड़ देता हूँ/
नंगी जमीन पर
कागज का कफन पहनाकर ।
वक्त /
कभी उसके तन पर /
अपनी सारी गर्द -
सुर्ख या स्याह,
शोहरत या इल्जाम -
जमा कर/ममी बना देता है.....
तो कभी
चील-कौओ के हवाले कर देता है........।
काश!
मैं उन बेजुबान मुर्दों की
ख्वाहिश जान पाता......।
जलाता नही/
जमीन मे गाड़ता नही/
ताबूतों मे भी कैद नही करता ;
छोड़ देता हूँ/
नंगी जमीन पर
कागज का कफन पहनाकर ।
वक्त /
कभी उसके तन पर /
अपनी सारी गर्द -
सुर्ख या स्याह,
शोहरत या इल्जाम -
जमा कर/ममी बना देता है.....
तो कभी
चील-कौओ के हवाले कर देता है........।
काश!
मैं उन बेजुबान मुर्दों की
ख्वाहिश जान पाता......।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
अपना हिस्सा
दिन मे सूरज उखड़ा-उखड़ा रहा,
रात मे चाँद भी रूठा सा रहा,
मैने जो माँग की,
अपने हिस्से के आसमां की ।
उड़ने की ख्वाहिश थी-
सो उड़ता रहा, भटकता रहा/
एक दिन /पैर टिकाने को
/जो थोड़ी सी जमीन माँगी /
वो भी अपने हिस्से की,
फिर सारे अपने नाता तोड़ गए,
संग जमीं के
वो भी मुझसे दूर हो गए..।
आज पैर हैं मेरे/
जमीन के कुछ उपर/
सर है आसमां के बहुत नीचे/
बीच मे लटका हुआमाँग रहा हूँ मैं-
अपने हिस्से की जमीं
अपने हिस्से का आस्मां.....।
रात मे चाँद भी रूठा सा रहा,
मैने जो माँग की,
अपने हिस्से के आसमां की ।
उड़ने की ख्वाहिश थी-
सो उड़ता रहा, भटकता रहा/
एक दिन /पैर टिकाने को
/जो थोड़ी सी जमीन माँगी /
वो भी अपने हिस्से की,
फिर सारे अपने नाता तोड़ गए,
संग जमीं के
वो भी मुझसे दूर हो गए..।
आज पैर हैं मेरे/
जमीन के कुछ उपर/
सर है आसमां के बहुत नीचे/
बीच मे लटका हुआमाँग रहा हूँ मैं-
अपने हिस्से की जमीं
अपने हिस्से का आस्मां.....।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
विडम्बना ,त्रासदी और सच्चाई
विडम्बना - मेरे जीवन की!
त्रासदी -एक विकृत मन की!
शायद !
खुद को बन्द कमरे में
लोगो की भीड़ में /
पहचान कीख्वाहिश रखता हूं... ,
जहाँ-भर की दुकानों को कोसकर
बाजारू नजरों में /खुद
ही नुमाइश बनता हूँ... ,
विडम्बना नहीं !त्रासदी नहीं !
यह तो सच्चाई है -
अन्तर्द्वन्द में फँसे /
विरोधाभासों से घिरे/
लोग अक्सर ऐसा ही सोंचते हैं ।
एक अंधेरी सुरंग के बीचोंबीच खड़ा मैं -
इधर भी रोशनी है,
उधर भी रोशनी है,
इस पार आने को भी दिल मचलता है
उधर का जहाँ देखने का भी मन करता है ...,
विडम्बना ही है,
त्रासदी ही है ,
और ये सच्चाई भी है -
दो खण्डो में बँटे /आधे-अधूरे /
लोग अक्सर ऐसी ही /
दोहरी जिन्दगी जिया करते हैं ।
त्रासदी -एक विकृत मन की!
शायद !
खुद को बन्द कमरे में
लोगो की भीड़ में /
पहचान कीख्वाहिश रखता हूं... ,
जहाँ-भर की दुकानों को कोसकर
बाजारू नजरों में /खुद
ही नुमाइश बनता हूँ... ,
विडम्बना नहीं !त्रासदी नहीं !
यह तो सच्चाई है -
अन्तर्द्वन्द में फँसे /
विरोधाभासों से घिरे/
लोग अक्सर ऐसा ही सोंचते हैं ।
एक अंधेरी सुरंग के बीचोंबीच खड़ा मैं -
इधर भी रोशनी है,
उधर भी रोशनी है,
इस पार आने को भी दिल मचलता है
उधर का जहाँ देखने का भी मन करता है ...,
विडम्बना ही है,
त्रासदी ही है ,
और ये सच्चाई भी है -
दो खण्डो में बँटे /आधे-अधूरे /
लोग अक्सर ऐसी ही /
दोहरी जिन्दगी जिया करते हैं ।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
Sunday, June 10, 2007
आज का मसीहा
आज का मसीहा ,
लटका होगा कहीं सलीब पर ,
और माँग रहा होगा दुआयें -
उनके लिये ,
जिन्होने इस हाल पर उसे पहुँचाया ..।
क्योंकि -
उन्ही की बदौलत ,
ये लोहे की जंजीरें ,
ये कीलें , ये सलीब ,
जिन्दा घाव , टीस उठाता दर्द ,
और इन्से मिलने वाली मौत -
उसकी अपनी और सिर्फ अपनी हो सकी ..।
लटका होगा कहीं सलीब पर ,
और माँग रहा होगा दुआयें -
उनके लिये ,
जिन्होने इस हाल पर उसे पहुँचाया ..।
क्योंकि -
उन्ही की बदौलत ,
ये लोहे की जंजीरें ,
ये कीलें , ये सलीब ,
जिन्दा घाव , टीस उठाता दर्द ,
और इन्से मिलने वाली मौत -
उसकी अपनी और सिर्फ अपनी हो सकी ..।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
मैं नहीं रोया
मैं नहीं रोया
आँखे खोली /
काली रात , स्याह पन्ने /
अरमान दफन हो गये / अन्धेरे का कफन ओढे /
उसी अन्धेरे में / धुल गई परछाईयाँ भी/
सपनों की मेरे .......।
फ़लक मेरा स्याह था,
सारा चरागाँ जो बुझ गया था..।
मेरे आँगन का चाँद /
दस्तक दे रहा था , किसी गैर दरवाजे पे/
परित्यक्त निशा को छोड़ गया
मेरे घर पे .........।
अंधेरे में कुछ बूँद आ टपके-
सोये से जागा मैं , फिर /
दिल को तसल्ली दे ली -
"रात ही रोई होगी बेचारी/
अपने चाँद के लिए .....,
साँसों के तार बन्धे हैं जिसके संग /
सजाता है आँखों में जो ख्वाबों के रंग /
उसी जान के लिए,
अपने चाँद के लिए.......।"
"रात ही रोई थी सचमुच !
मैं कैसे रो सकता हूँ /
इन्सान हूँ जो....,
बचपन से ही सिखाया गया है-
जो दूसरे की है , वो अपनी नहीं हो सकती /
हाँ , गर अपनी गैर की हो जाए ,तो
रोना नहीं , आँसू दिखाना नहीं /
इन्सान तो दूसरों के वास्ते ही जीता है ,
वरना हैवान ना कहलाता वो .......।"
"वो क्या जाने बड़ी-बड़ी बातें -
वो तो हँस जाती है खुशी में ,
गीली हो उठती है गम में /
कितनी भोली है, शायद सुखी भी,
अपनी खुशी खुद जी पाती है,
अपना रोना खुद रो पाती है ।"
सच में अब लगने लगा है -
रात ही रोई थी शायद ।
आँखे खोली /
काली रात , स्याह पन्ने /
अरमान दफन हो गये / अन्धेरे का कफन ओढे /
उसी अन्धेरे में / धुल गई परछाईयाँ भी/
सपनों की मेरे .......।
फ़लक मेरा स्याह था,
सारा चरागाँ जो बुझ गया था..।
मेरे आँगन का चाँद /
दस्तक दे रहा था , किसी गैर दरवाजे पे/
परित्यक्त निशा को छोड़ गया
मेरे घर पे .........।
अंधेरे में कुछ बूँद आ टपके-
सोये से जागा मैं , फिर /
दिल को तसल्ली दे ली -
"रात ही रोई होगी बेचारी/
अपने चाँद के लिए .....,
साँसों के तार बन्धे हैं जिसके संग /
सजाता है आँखों में जो ख्वाबों के रंग /
उसी जान के लिए,
अपने चाँद के लिए.......।"
"रात ही रोई थी सचमुच !
मैं कैसे रो सकता हूँ /
इन्सान हूँ जो....,
बचपन से ही सिखाया गया है-
जो दूसरे की है , वो अपनी नहीं हो सकती /
हाँ , गर अपनी गैर की हो जाए ,तो
रोना नहीं , आँसू दिखाना नहीं /
इन्सान तो दूसरों के वास्ते ही जीता है ,
वरना हैवान ना कहलाता वो .......।"
"वो क्या जाने बड़ी-बड़ी बातें -
वो तो हँस जाती है खुशी में ,
गीली हो उठती है गम में /
कितनी भोली है, शायद सुखी भी,
अपनी खुशी खुद जी पाती है,
अपना रोना खुद रो पाती है ।"
सच में अब लगने लगा है -
रात ही रोई थी शायद ।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
कब्र की मिट्टी
कब्र की मिट्टी
अंधेरी रातों मे / दफन होता मेरा सूरज/
चीखता है, चिल्लाता है,
आवाज जा उफक तक/ लौट आती है ।
कोई सुन पाता नहीं !
कोई जान पाता नहीं !
सुनेगा भी तो कौन -
मेरी धरती / ख्वाबों में /
अपने आसमान को,
उसी उफक पर/बस /
छू भर रही होती है ।
जानेगी भी तो क्या होगा -
फ़कत रस्मोंअदायगी को/
स्वप्निल बन्द आँखें लिए/
अपना सर ढँके/
डाल आएगी / उसकी कब्र पर /
ताजी भुरभुरी मिट्टी ।
उसे क्या पता है -
जागेगी नींद से जब वो/
आँखे खोलने ना पायेगी ।
पलकों पर जो रखी है/
वही/ उसकी अपनी/
ताजी भुरभुरी मिट्टी ।
अंधेरी रातों मे / दफन होता मेरा सूरज/
चीखता है, चिल्लाता है,
आवाज जा उफक तक/ लौट आती है ।
कोई सुन पाता नहीं !
कोई जान पाता नहीं !
सुनेगा भी तो कौन -
मेरी धरती / ख्वाबों में /
अपने आसमान को,
उसी उफक पर/बस /
छू भर रही होती है ।
जानेगी भी तो क्या होगा -
फ़कत रस्मोंअदायगी को/
स्वप्निल बन्द आँखें लिए/
अपना सर ढँके/
डाल आएगी / उसकी कब्र पर /
ताजी भुरभुरी मिट्टी ।
उसे क्या पता है -
जागेगी नींद से जब वो/
आँखे खोलने ना पायेगी ।
पलकों पर जो रखी है/
वही/ उसकी अपनी/
ताजी भुरभुरी मिट्टी ।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
विवशता
विवशता
समाज की नंगी तस्वीर जो देखी ,
मुठ्ठियाँ कसी , नथुने फूले ,
रगों में लावा सा दौड़ने लगा ।
रक्ताभ आँखों ने सच्चाई देखी ,
भीड़ के सामने मैं अकेला खड़ा था...।
मैं निहत्था ,वे जत्थेदार हथियारबन्द ,
चारो ओर से बढता कोलाहल-
डर लगने लगा और
यथार्थ ने ला धरती पे पटका .....।
माथे पर सिलवटें पड़ी ,
मुठ्ठियाँ खुल गई ,
हथेलियाँ जुड़ गई
और सर उन पर टिक गया...।
क्या करता -
विवशता दस्तक दे चुकी थी...।
समाज की नंगी तस्वीर जो देखी ,
मुठ्ठियाँ कसी , नथुने फूले ,
रगों में लावा सा दौड़ने लगा ।
रक्ताभ आँखों ने सच्चाई देखी ,
भीड़ के सामने मैं अकेला खड़ा था...।
मैं निहत्था ,वे जत्थेदार हथियारबन्द ,
चारो ओर से बढता कोलाहल-
डर लगने लगा और
यथार्थ ने ला धरती पे पटका .....।
माथे पर सिलवटें पड़ी ,
मुठ्ठियाँ खुल गई ,
हथेलियाँ जुड़ गई
और सर उन पर टिक गया...।
क्या करता -
विवशता दस्तक दे चुकी थी...।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
लाचारी
लाचारी
मुठ्ठी में आस्माँ समेटने की सोंची थी ,
कुछ भी हो -
’फ़लक कल्पना से बड़ा हो ,
या बस शून्य का मायाजाल ’
होना तो वही था -
सिवा सिफर के कुछ नहीं था मेरे पास /
हाथ खाली के खाली ही रहे ...।
अब,
अनन्त को बाँध सकता नहीं/
शून्य को समेट पाता नहीं ,
तरस आता है /
अपनी लाचारी पे -
"कूबत नहीं है जब ,
तो क्यूँ सोंचता है -
किसी को अपना बनाने को....,
खालीपन में जा भरने को किसी के/
या विस्तार में जा विलीन हो जाने को..।"
मुठ्ठी में आस्माँ समेटने की सोंची थी ,
कुछ भी हो -
’फ़लक कल्पना से बड़ा हो ,
या बस शून्य का मायाजाल ’
होना तो वही था -
सिवा सिफर के कुछ नहीं था मेरे पास /
हाथ खाली के खाली ही रहे ...।
अब,
अनन्त को बाँध सकता नहीं/
शून्य को समेट पाता नहीं ,
तरस आता है /
अपनी लाचारी पे -
"कूबत नहीं है जब ,
तो क्यूँ सोंचता है -
किसी को अपना बनाने को....,
खालीपन में जा भरने को किसी के/
या विस्तार में जा विलीन हो जाने को..।"
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
अस्तित्व-बोध
अस्तित्व - बोध
टुकड़ो में बँटती जिन्दगी / अस्तित्वहीन होता अन्तस /
एक सूनापन ; एक खालीपन /
फिर भी जिये जा रहा हूँ ........,
नियति से बँधी /
एक परिणति की आस में /
साँस लिये जा रहा हूँ .......... ।
खोज जारी है,तलाश जारी है,
अपने पहचान की , एक इन्सान की .... ।
दिल में टीस सी उठती है /
रोता हूँ , कराह पाता नहीं /
बेदखल हूँ / अपने ही घर से /कोने मे दुबके बूढे की तरह/
उखड़ी साँसों को थामता हूँ -
आवाज ना कोइ आने पाए ,
कहीं कोई नींद ना खुल जाए .....।
खोज जारी है,तलाश जारी है,
अपने पहचान की , एक इन्सान की .... ।
कदम ठिठकते हैं / चेतना की गाँठ खुलती है /
टुकड़े पड़े हैं सामने /
तलाश रहा हूँ एक आस लिए -
शायद मेरे नाम का टुकड़ा कहीं दिख जाए,
पल-भर को ही सही ,
मुझे मेरा अस्तित्व-बोध करा तो जाए......।
खोज जारी है,तलाश जारी है,
अपने पहचान की , एक इन्सान की .... ।
टुकड़ो में बँटती जिन्दगी / अस्तित्वहीन होता अन्तस /
एक सूनापन ; एक खालीपन /
फिर भी जिये जा रहा हूँ ........,
नियति से बँधी /
एक परिणति की आस में /
साँस लिये जा रहा हूँ .......... ।
खोज जारी है,तलाश जारी है,
अपने पहचान की , एक इन्सान की .... ।
दिल में टीस सी उठती है /
रोता हूँ , कराह पाता नहीं /
बेदखल हूँ / अपने ही घर से /कोने मे दुबके बूढे की तरह/
उखड़ी साँसों को थामता हूँ -
आवाज ना कोइ आने पाए ,
कहीं कोई नींद ना खुल जाए .....।
खोज जारी है,तलाश जारी है,
अपने पहचान की , एक इन्सान की .... ।
कदम ठिठकते हैं / चेतना की गाँठ खुलती है /
टुकड़े पड़े हैं सामने /
तलाश रहा हूँ एक आस लिए -
शायद मेरे नाम का टुकड़ा कहीं दिख जाए,
पल-भर को ही सही ,
मुझे मेरा अस्तित्व-बोध करा तो जाए......।
खोज जारी है,तलाश जारी है,
अपने पहचान की , एक इन्सान की .... ।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
वजूद
परछाईयों का शहर /
तन्हाई का सफर /हमसफर ढूँढा /
धूल सने हाथों में सिफर उभर आया ।
समझ गया -
साये कभी औरों के नहीं होते ।
देते हैं गवाही मेरे होने की,
जो घटती-बढती छाया में अपना कद नापता हूँ ,
सपनों की पगडंडियों पर चलता ,
किसी लौ में अपना वजूद ढूँढता हूँ ।
तन्हाई का सफर /हमसफर ढूँढा /
धूल सने हाथों में सिफर उभर आया ।
समझ गया -
साये कभी औरों के नहीं होते ।
देते हैं गवाही मेरे होने की,
जो घटती-बढती छाया में अपना कद नापता हूँ ,
सपनों की पगडंडियों पर चलता ,
किसी लौ में अपना वजूद ढूँढता हूँ ।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
Monday, June 4, 2007
Confusion
खुद को मिटाने चला था /
कूदते-कूदते एक प्रतिबिम्ब दिखा ;
मेरा अपना सा लग रहा था ,
पूछ रहा था -
"मरना क्यूँ चाहते हो ? "
.....................................
.....................................
....................................
अनन्त बालुकाराशि / तपता सूरज /
वही प्यासा मृग / वही मरीचिका ;
छाया , किसी गैर की ,
पूछ रही थी -
" जीना क्यूँ चाहते हो ? "
.....................................
.....................................
.....................................
ना जीने का अर्थ जान पाया,
ना मरने का मर्म समझ में आया /
फलसफों में घुटता रहा,
ना जी पाया , ना मर पाया ।
कूदते-कूदते एक प्रतिबिम्ब दिखा ;
मेरा अपना सा लग रहा था ,
पूछ रहा था -
"मरना क्यूँ चाहते हो ? "
.....................................
.....................................
....................................
अनन्त बालुकाराशि / तपता सूरज /
वही प्यासा मृग / वही मरीचिका ;
छाया , किसी गैर की ,
पूछ रही थी -
" जीना क्यूँ चाहते हो ? "
.....................................
.....................................
.....................................
ना जीने का अर्थ जान पाया,
ना मरने का मर्म समझ में आया /
फलसफों में घुटता रहा,
ना जी पाया , ना मर पाया ।
 An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
An engineer(IITian) by qualification, educationist by profession and mythologist by passion. He fathoms up to the deeper roots of mythological stories and wisdom enshrined in our Sanatana dharma texts like Vedas, Puranas, Epics and specially Gita. He is a naturally gifted speaker and enthrall the audience with the waves of his rhythmic intonation and way of story-telling.
Subscribe to:
Posts (Atom)