सो बाबूजी की शरीर की घड़ी बड़ी ही धीमी हो गई है। उनके दिन-रात थोड़े लंबे हो गए हैं। जितने समय में उनके मानसिक जगत का सूरज और चांद एक-एक बार उगता और डूबता है, उतनी देर में दीवार पर टंगी घड़ी की सुईयां कभी चार तो कभी छः चक्कर लगा लेती है। बाबूजी अपनी घड़ी से चलते हैं और दुनिया वाली घड़ी से चलना हमारी आदत और मजबूरी दोनों है।
पेंडुलम वाली घड़ी के धीमी होने के पीछे विज्ञान एक बड़ा ही interesting explaination देता है - या तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ गई हो या उस पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया हो। मजे की बात यह भी है कि वही बल उस पेंडुलम को लगातार oscillate भी करवाता रहता है। जन्म और मृत्यु की extreme नियति के बीच में डोलते इंसान की भी यही कैफियत है। 'अहंता' पेंडुलम की लंबाई निर्धारित करती है और 'ममता' उसे गतिशील रहने के लिए बल प्रदान करती है।
बाबूजी जैसे ऊंची शख्सियत वाले व्यक्तित्व की 'लंबाई' नहीं मापी जाती, उनका 'कद' मापा जाता है। वो ऊँचा कद, जो उन्होने अपने अथक प्रयासों से जीवन भर में establish किया। वह ऊँचा कद, जिसकी छाया से अभी तक हम निकल पाने में सक्षम नहीं हुए हैं और भविष्य में शायद कभी हो भी नहीं पाएंगे। 1980 तथा 1990 के दशक में बिहार में B.Ed करने वाले सभी छात्र-छात्राओं के लिए डॉ सच्चिदानंद सिंह का नाम अनसुना नहीं होगा। करीब 2 दशकों तक उनकी लिखी किताबें Teacher's Training के स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती आईं। जहाँ शैक्षणिक उपाधियों से उनकी किताबों में लेखक- परिचय का पूरा पृष्ठ भर जाता था, उस कद को उनका यह केवल स्नातक-उर्तीण ( B.Tech. only)बेटा केवल गर्व और सम्मान से ही तो देख सकता है।
पूरी तरह involve होकर अपने दम पर अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा ली। सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। बेटियों की शादी कर दी, बेटों को अपने पैरों पर खड़ा करवा दिया। हमारे ऊपर खुद का जीवन गुजारने के अलावा कोई बोझ नहीं छोड़ा। और फिर सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन्होंने बिल्कुल ठीक समय पर खुद को बहुत सारे जाल-जंजालों से मुक्त कर लिया। अपने अनुसार यथाशक्ति सबको अपना अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता दे दी। 'ममता' की आसक्ति के बल को एक स्थितप्रज्ञ योगी की भांति deliberately धीरे-धीरे क्षीण करते चले गए। जैसे-जैसे स्मरण शक्ति घटती जा रही है, वैसे वैसे यह प्रक्रिया और accelerated होती जा रही है। लोगों को पहचानना भी धीरे-धीरे अनिश्चित होता जा रहा है। अपनी ही बनाई धरती से मोह कम होता जा रहा है।
भौतिकी की वही दिलचस्प शै याद आ रही है। इतने अच्छे से तो व्याख्या की थी- " कि घड़ी कैसे धीमी होती चली जाती है।" फार्मूला है, लगता ही रहेगा- अपने सारे limitations के बावजूद भी। हम denial की कितनी भी कोशिश कर लें, प्रकृति तो अपना काम करेगी ही। कल को हम सब की घड़ी mis-match होगी।
#

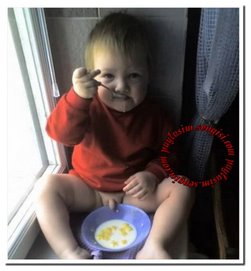
No comments:
Post a Comment